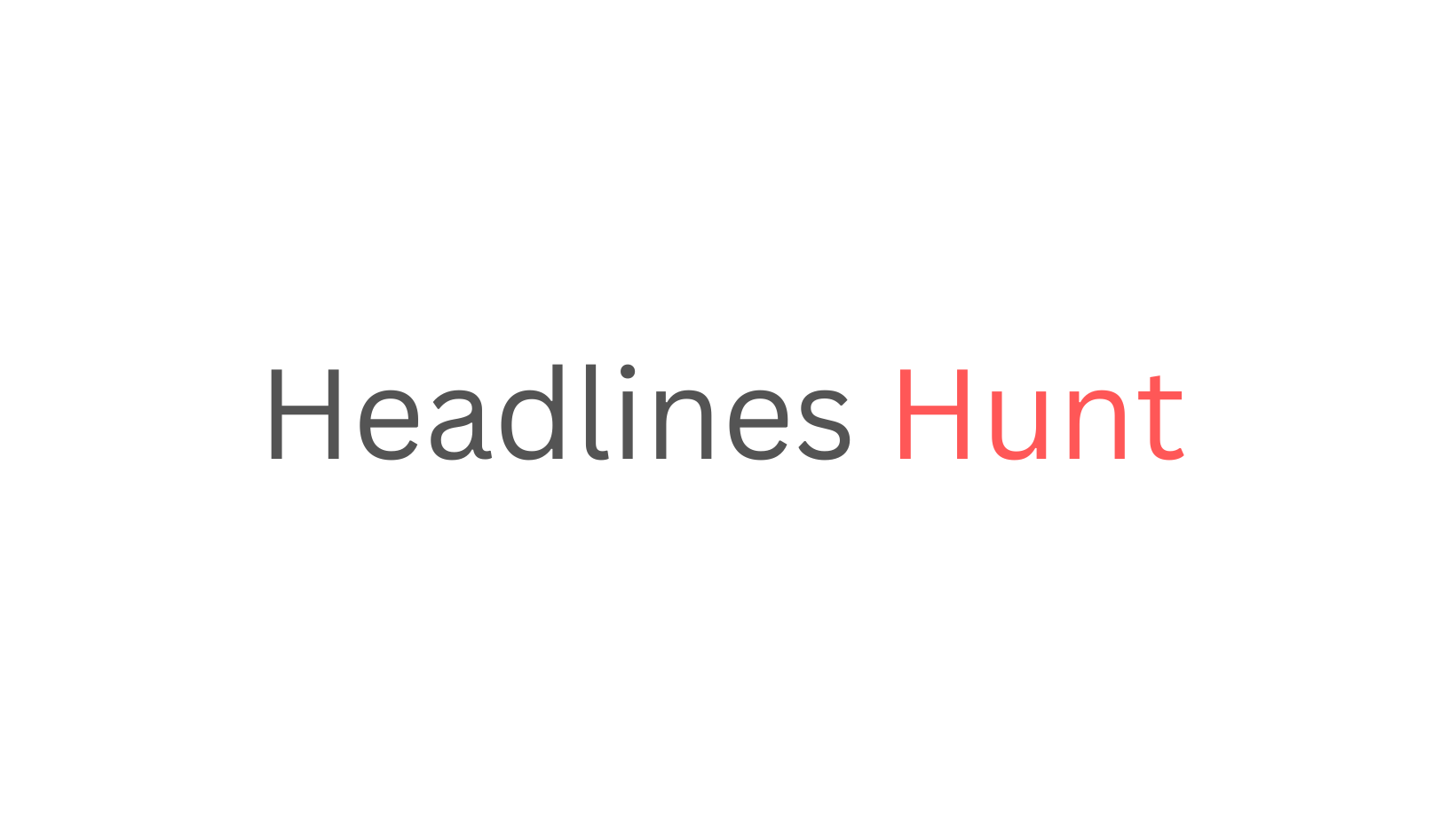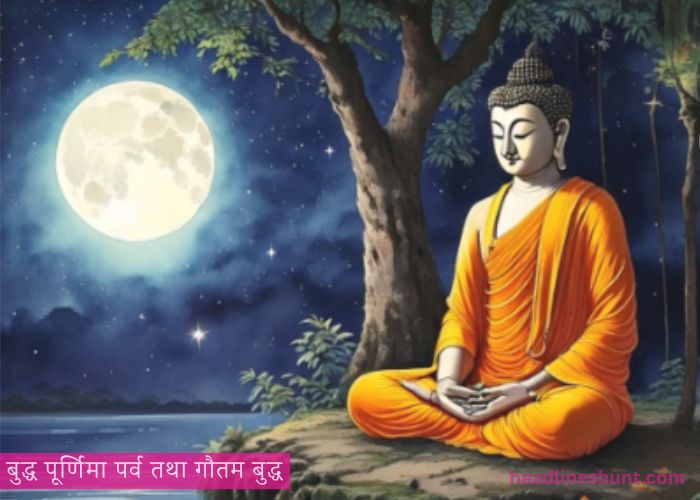
बुद्ध पूर्णिमा पर्व तथा गौतम बुद्ध
बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, बैशाख पूरणमासी भी कहा जाता है, हिन्दू विक्रमी सम्वत पंचांग के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन को कहा जाता है, इसी दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है.
हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के पावन दिन पर भगवान विष्णु और चंद्रमा की भी विधि- विधान से पूजा- अर्चना की जाती है. पूर्णिमा तिथि को हिंदी पंचांग में महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दिन चन्द्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, जो पूर्णिमा को निर्मल, शीतल एवं शांत बनाता है.
इसी उत्तम तिथि को जन्में बुद्ध के जीवन पर भी पूर्णिमा का गहरा प्रभाव रहा है, और वैसा ही बुद्ध का स्वभाव भी बना. भगवान बुद्ध को विष्णु भगवान का नौवां अवतार भी माना जाता है.
बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है, साथ ही इस दिन श्रद्धालु इस दिन विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधि, जैसे ध्यान, पूजा, और दान आदि के माध्यम से भी भगवान बुद्ध को भी याद करते है. इस दिन बहुत से बौद्ध उपासक ऊपोसथ व्रत धारण करते हुए शील, सदाचार और सत्कर्म पर आरूढ़ होने का संकल्प लेते है.
भगवान गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य विचारों के जरिए समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा था और समाज में सकारात्मक परिवर्तन किये थे. ज्ञान और भक्ति की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्त्व देने की शिक्षा देने वाले गौतम बुद्ध ने कर्म को बहुत सोच - समझ कर अपना धर्म-मार्ग बनाया था. वे करुणा, दया, अहिंसा और मित्रता की पैरवी करते थे.
महात्मा गौतम बुद्ध को तथागत बुद्ध, शाक्यमुनि, लाइट ऑफ एशिया जैसे उप नामों से भी जाना जाता है.
गौतम बुद्ध के सानिध्य में जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति आया, उनकी सम्यक दृष्टि पाकर उन्हीं की तरह निर्मल, शीतल एवं शांत हो गया.
भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति जिसे बुद्धत्व या संबोधि कहा जाता है और उनका महापरिनिर्वाण ये तीनों महान संयोग वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे. इसीलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी विश्वभर में बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं.
563 ई.पू. में बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम, शाक्य राज्य जो आज नेपाल है, में हुआ था. जन्म के समय उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ नाम दिया गया था. गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था. गौतम बुद्ध की माता का देहांत उनके जन्म के तुरंत बाद हो गया जिसके बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन-पोषण किया था. जिसके बाद 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ. यशोधरा और गौतम बुद्ध के एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था.
विवाह के बाद जब मानव जीवन के दुखों जैसे रोग, वृद्धावस्था एवं मृत्यु इत्यादि को गौतम बुद्ध ने जब देखा, तो वह विचलित हो गए, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर जीवन के सत्य की तलाश में गौतम बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया.
घर छोड़ने की यह प्रक्रिया बाद में बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से पहचानी गयी. घर छोड़ने के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ को लगभग 7 वर्ष तक इधर-उधर भटकना पड़ा. इस दौरान उन्होंने उदक रामपुत्र, अलार कलाम से सांख्य दर्शन, की दीक्षा दी. फिर उन्होंने उरुवेला बोधगया की और प्रस्थान किया था, जहां बुध की मुलाकात कौडिन्य समेत पांच संन्यासियों से हुई थी.
35 वर्ष की आयु में, उरुवेला बोधगया (वर्तमान में बिहार, भारत) में ही निरंजना नदी के तट पर स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिन की समाधि के बाद गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के ही दिन ज्ञान का बोध बुद्धत्व (सम्यक ज्ञान) प्राप्त हुआ था. इसके बाद से यह वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा. यह ज्ञान प्राप्ति का समय बुद्ध की जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था. ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने वाराणसी के समीप अपने पांच शिष्यों को उपदेश दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया.
इसके बाद मगध को आधार बनाते हुए गौतम बुद्ध ने कई महाजनपदों की यात्रा की और लोगों को उपदेश दिया. तब गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्रभाव से ही मगध का शासक बिंबिसार, कौशांबी का राजा उदयन तथा कौशल का राजा प्रसेनजीत भी उनका अनुयाई था.
जिस समय भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था, तब लोग धीरे धीरे वेदों से विमुख होने लगे थे और नया समाज विलासिता को वरीयता देने लगा था. इस सब के चलते एक अंतहीन दौड़ का सिलसिला शुरू हुआ जिसने समाज को अव्यवस्थित,और अशांत कर दिया. ऐसे में लोग शांति पाने के लिए वेदों के अतिरिक्त कहीं और से शांति कि तलाश में भटकने लगे, साथ ही जानवरों कि बलि जैसी कुप्रथाएं शुरू हो गई और आगे बढ़ने कि होड़ में इंसान इंसान का ही दुश्मन होने लगा.
ऐसी परिस्थितियों में अशांत मन में लोग एक दूसरे की हत्या लूटपाट तक करने लगे थे, तब भगवान बुद्ध ने शांति और त्याग का मार्ग अपनाते हुए समय को सही सन्देश दिया, इसमें लोगों को शांति दिखी और फिर बहुत तेजी से बौद्ध धर्म न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी खूब फैला.
गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में चुन्द द्वारा अर्पित भोजन को ग्रहण करने के बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के एक कस्बे कुशीनगर, जिसका उल्लेख इतिहास में कुुशनारा नाम से मिलता है, में शरीर का त्याग कर दिया था. जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है. महापरिनिर्वाण के उपरांत महात्मा गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके भारत के अलग-अलग स्थानों पर स्थापित करके उनपर स्तूपो का निर्माण कराया गया.
गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का स्वरूप लोकतंत्र वादी रखा गया, जिसका उद्देश्य बहुजन हिताय था. बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्न है-
चार आर्य सत्य
1. दुक्खम अर्थात दुःख है.
2. समुदाय अर्थात दुःख के कारण हैं.
3. निरोधः अर्थात दुःख के निवारण हैं.
4. निरोधगामिनी प्रतिपदः अर्थात दुखों के समुदाय के नाश (निरोध ) हेतु मार्ग ( प्रतिपद ) हैं .यानि दुःख-निवारण के उपाय हैं.
इन्हीं दुखों के निवारण हेतु महात्मा गौतम बुद्ध निरोधगामिनी प्रतिपद के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग के अनुपालन करने को कहा -
1. सम्यक- दृष्टि
2. सम्यक- संकल्प
3. सम्यक- वचन
4. सम्यक -कर्म
5. सम्यक -आजीविका
6. सम्यक -व्यायाम
7. सम्यक -स्मृति
8. सम्यक -समाधि
महात्मा गौतम बुद्ध ने मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण को बताया, और निर्वाण की प्राप्ति हेतु आचरण की शुद्धता पर अधिक बल दिया. इसके लिए उन्होंने 10 शीलों के पालन को आवश्यक बताया, इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय(चोरी न करना), अपरिग्रह(धन संग्रह न करना), ब्रह्मचर्य, नृत्य व संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, उस समय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग आदि व्यवहारों का अनुकरण करने के लिए कहा गया. उपरोक्त में से प्रथम पांच गृहस्थ लोगों के लिए तथा बौद्ध भिक्षु के लिए सभी 10 शील अनिवार्य थे.
बौद्ध धर्म के तीन रत्न – बुद्ध, धम्म, संघ
महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए दर्शन -
क्षणिकवाद- महात्मा बुद्ध संसार को क्षणभंगुर एवं परिवर्तनशील मानते थे.
अनीश्वरवाद- गौतम बुद्ध अनीश्वरवाद को मानते हुए ईश्वरीय सत्ता को नकार देते.
प्रतीत्यसमुत्पाद- इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु के विनाश के उपरांत दूसरे की उत्पत्ति होती है, प्रत्येक घटना के पीछे कार्य-कारण सिद्धांत होता है.
कर्मवाद- बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे एवं यज्ञ, पूजा, बलिदान को निरर्थक मानते हुए कर्म को फलों का आधार मानते थे.
अनात्मवाद- गौतम बुद्ध ने आत्मा को स्वीकार नहीं किया एवं मनुष्य के व्यक्तित्व को कुछ संस्कारों के समूह को मानते थे.
पुनर्जन्म- ईश्वर और आत्मा पर विश्वास न रखने के बावजूद बुद्ध पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, हालांकि उनका मानना था कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि अनित्य अहंकार का होता है.
निर्वाण- गौतम बुध के अनुसार निर्वाण एक ऐसी अवस्था होती है जहां ज्ञान की ज्योति द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार की समाप्ति हो जाती है.
महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा किये गए सामाजिक धार्मिक सुधार-
गौतम बुद्ध ने तात्कालिक समाज में सुधार करने के लिए निम्न पक्षों पर ध्यान दिया
कर्मकांड, यज्ञ तथा पशु बलि का विरोध
जात पात का खंडन
अहिंसा पर अत्यधिक बल
वेदों में अविश्वास
बौद्ध संगीतियां
- प्रथम बौद्ध संगीति- राजगृह (सप्तपर्णी गुफा) अध्यक्ष– महाकस्सप, शासनकाल– अजातशत्रु (हर्यक वंश)
- द्वितीय बौद्ध संगीति- वैशाली, अध्यक्ष – साबकमीर (सर्वकामनी), कालाशोक (शिशुनाग वंश)
- तृतीय बौद्ध संगीति- पाटलिपुत्र, अध्यक्ष – मोग्गलिपुत्ततिस्स, अशोक (मौर्यवंश)
- चतुर्थ बौद्ध संगीति- कश्मीर के कुण्डलवन, अध्यक्ष – वसुमित्र, उपाध्यक्ष – अश्वघोष, शासनकाल – कनिष्क (कुषाण वंश)
महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य
त्रिपिटक- त्रिपिटक को बौद्ध साहित्य का मूल ग्रंथ माना जाता है. इसमें गौतम बुद्ध के मूल विचारों से लेकर बौद्ध धर्म के नियम और दर्शन भी सम्मिलित है.
1. विनय पिटक (बौद्ध संघ के नियम एवं विधान)
2. सुत्त पिटक (महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा विचार)
3. अभिधम्म पिटक (बौद्ध दर्शन)
जातक- भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं
महावस्तु और अंगुत्तर निकाय निकाय- 16 महाजनपदों का वर्णन
बुद्धचरितम- अश्वघोष द्वारा रचित, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश
महावंश और दीपवंश- गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालने वाली श्रीलंका साहित्य
मिलिंदपन्हो- इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णन
दिव्यदान- अशोक और कुणाल से संबंधित
बुद्ध से सम्बंधित प्रतीक :
- हाथी: बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक
- कमल: जन्म का प्रतीक
- साढ : यौवन का प्रतीक
- घोड़ा: गृह त्याग का प्रतीक
- पीपल: ज्ञान का प्रतीक
- शेर: समृद्धि का प्रतीक
- पदचिन्ह: निर्वाण का प्रतीक
- स्तूप: मृत्यु का प्रतीक
Read more at headlineshunt :
 भुवनेश्वर कुमार का जीवन परिचय
भुवनेश्वर कुमार का जीवन परिचय माता दुर्गा के परम भक्त साधक सुदर्शन जी
माता दुर्गा के परम भक्त साधक सुदर्शन जी पितृ पक्ष में कौवें को खाना खिलाने का वैज्ञानिक महत्त्व
पितृ पक्ष में कौवें को खाना खिलाने का वैज्ञानिक महत्त्व आयुष बडोनी का जीवन परिचय
आयुष बडोनी का जीवन परिचय आदिशक्ति भवानी माँ दुर्गा
आदिशक्ति भवानी माँ दुर्गा प्रिया सिंह मेघवाल द फेमस बॉडी बिल्डर
प्रिया सिंह मेघवाल द फेमस बॉडी बिल्डर अदिति जेटली जडेजा वाइफ ऑफ अजय जडेजा
अदिति जेटली जडेजा वाइफ ऑफ अजय जडेजा सिद्धारमैया कर्नाटक की राजनीती के बड़े खिलाडी
सिद्धारमैया कर्नाटक की राजनीती के बड़े खिलाडी अनसूया सेनगुप्ता एन एक्ट्रेस एंड प्रोडक्शन डिज़ाइनर
अनसूया सेनगुप्ता एन एक्ट्रेस एंड प्रोडक्शन डिज़ाइनर कल्पना मुर्मू सोरेन वाइफ ऑफ हेमंत सोरेन
कल्पना मुर्मू सोरेन वाइफ ऑफ हेमंत सोरेन रेहाना फातिमा फेमस फेमिनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट
रेहाना फातिमा फेमस फेमिनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट देवेंद्र फडणवीस का जीवन परिचय
देवेंद्र फडणवीस का जीवन परिचय शरद पवार का जीवन परिचय
शरद पवार का जीवन परिचय सुजाता सौनिक का जीवन परिचय
सुजाता सौनिक का जीवन परिचय ब्रज भूषण शरण सिंह का जीवन परिचय
ब्रज भूषण शरण सिंह का जीवन परिचय